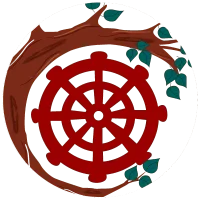दिवंगत विद्वान राइस डेविड्स द्वारा दिया गया यह कथन (यहाँ पर भावानूदित की गई है) बुद्ध के बारे में सबसे लोकप्रिय भ्रांतियों में से एक है। इस कथन में दो त्रुटियाँ हैं: सबसे पहले, हिंदू या हिंदू धर्म जैसे शब्दों की उत्पत्ति हाल ही में हुई जो बुद्ध के समय मौजूद नहीं थे। वैदिक प्रणाली में विश्वास करने वालों और इसके मतों या षड्दर्शन को अंगीकार करने वालों ने आधुनिक युग तक खुद की पहचान के लिए इस शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं किया। वस्तुतः यह विदेशी द्वारा प्रयोग किया गया एक शब्द था जिसे विशेष रूप से मुसलमानों द्वारा गैर-इस्लामी लोगों को इंगित करने के लिए किया जाता था जो सिंधु नदी से परे रहते थे। हालाँकि इस शब्द को अपनी आधिकारिक मुहर तब मिली जब ब्रिटिश प्रवासीय अधिकारियों ने हिंदुओं और मुसलमानों को दो धर्म समूहों के रूप में विभाजित किया और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उन्होंने इन शब्दों को कानूनी रुप से वैध कर दिया। बदले में थियोसोफिकल सोसायटी के संस्थापक सदस्य एनी बेसेंट ने १८८९ ईस्वी में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की और १९१० में अन्य हिंदू विद्वानों के साथ मिलकर “सनातन धर्म, हिंदू धर्म और नैतिकता की एक प्राथमिक पाठ्यपुस्तक” (Sanatana Dharma, An Elementary Textbook of Hindu Religion and Ethics) नामक एक पुस्तक लिखी, जिसने अंततः हिंदू शब्द को एक प्रशासनिक नामकरण से अधिक अर्थ दिया – इस शब्द को एक धार्मिक अर्थ मिला। इस तरह इस शब्द ने धार्मिक आवरण भी ग्रहण किया और बाद में भारतवर्ष की वैदिक परम्परा में विश्वास रखने वालों को इसी शब्द से पहचाना गया। अब इस शब्द का प्रयोग वैदिक धारा के संग जन्मे और हजारों वर्षों की अवधि में प्राचीन भारत में विकसित हुए अनेकानेक धार्मिक सिद्धांतों और प्रयासों को अपने में समाहित करते आए धार्मिक मतों के मिश्रण को परिचित कराने के लिए किया जाता है। बुद्ध के समय में न तो हिन्दू नामक शब्द ही था और ना ही हिन्दुधर्म। उस समय में केवल “वैदिक ब्राह्मणवाद” था।
अब दूसरा मुद्दा यह है कि क्या बुद्ध का जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जो वैदिक ब्राह्मणवाद का अभ्यास करते थे और क्या उन्होंने अपने समय के वैदिक ग्रंथों में लिखी शिक्षाओं को सिखाना जारी रखा। पाली ग्रन्थ (थेरवाद), चिनिया भाषामें अनुवादित सर्वास्तिवादी आगम तथा विभिन्न महायानसूत्रों में संगृहीत बुद्ध की शिक्षाएं एक अलग ही कहानी बयान करते हैं। इसके अनुसार सिद्धार्थ गौतम ऐसे परिवार से ताल्लुक नहीं रखते थे जो वैदिक प्रथाओं का सख्ती से पालन करते थे और न ही उनके कुल वैदिक आचार-संस्कारों का पालन करते थे जो बाद में चल कर मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में सूत्रबद्ध हुआ। हमें बौद्ध और वैदिक दोनों स्रोतों से सूचित किया जाता है कि शाक्य वंश वैदिक प्रभावों के दायरे से कुछ बाहर था। मनु स्मृति के दसवें अध्याय में यह उल्लेखित है कि शाक्य-क्षेत्र में वैदिक वर्णव्यवस्था से पतन हुए मिश्रित समुदाय का (वर्णसंकर) बसोबास था। इसकी पुष्टि बौद्ध ग्रंथों जैसे अम्बट्ठ सुत्त से भी होती है जिसमें एक वैदिक शिक्षा में पारंगत युवा ब्राह्मण, जिसका नाम अम्बट्ठ था, बुद्ध से शिकायत करता है, “शाक्य लोग ब्राह्मणों का सम्मान ठीक से नहीं करते हैं। वे असभ्य, तुच्छ और कटुवाणीयुक्त हैं।” इसलिए बुद्ध को वैदिक परिवार में पैदा हुए व्यक्ति के रूप में संदर्भित करने का कोई मतलब नहीं है।
फिर भी बुद्ध ने स्वयं को क्षत्रिय होने का उल्लेख किया जिसके लिए हमें समाज में वर्गों के विकासकर्म पर बुद्ध के विचारों की जांच करने की आवश्यकता होगी। अगञ्ञ सुत्त जो संसार उत्पत्ति के सम्बन्ध में बौद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, इसमें बुद्ध उल्लेख करते हैं कि ये वर्ग (जो बाद में वर्ण व्यवस्था के रुपमे बिकासित हुवा) समाज में कैसे प्रकट हुए। अगञ्ञ सुत्त के अनुसार वर्ग किसी जन्म या किसी शास्त्र के प्रतिबंधों के आधार पर नहीं बल्कि केवल आवश्यकता और व्यवसाय के आधार पर बने हैं। इस सुत्त में बुद्ध के अनुसार मनुष्यों के पहले निर्वाचित राजा, “महासम्मत” को लोगों द्वारा और लोगों के लिए कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए चुना गया था। मानव जगत में “क्षत्रिय वर्ग” का यह विचार पहली बार जन्म के आधार पर न होकर व्यक्ति की गुणवत्ता और उसके स्वयं के व्यवसाय के आधार पर विकसित हुआ। ‘महावंश’ जैसे बौद्ध ग्रंथों का दावा है कि शाक्य वंश ऐसे ही प्रथम राजा “महासम्मत” के वंशज थे जो अपने पिछले जीवन में बोधिसत्व हुआ करते थे। इसके अलावा बुद्ध बताते हैं कि उसी समाज के लोगों में से कुछ लोगों ने मानव समाज से खुद को अलग करते हुए एक सात्विक और शुद्ध जीवनशैली को बनाए रखना शुरू किया; वे जंगल में दिन रात ध्यान करते हुए रहना पसंद करते थे। उन्हीं लोगों को “ब्राह्मण” कहा गया।
ऐसे कुछ सूत्त हैं जिनमें बुद्ध ने ऐसे प्राचीन ब्राह्मणों और उनके अभ्यासों की प्रशंसा का उल्लेख किया है। इस तरह के विचारों पर आधारित होकर बुद्ध ने खुद को “क्षत्रिय” कहा और जन्म के आधार पर कठोर जाति व्यवस्था या वैदिक ग्रन्थ में कहे अनुसार किसी आदिपुरुष (जैसा कि ऋग्वेद के पुरुष सूत्त में उल्लेख किया गया है ) के शरीर के अंग से उनकी उत्पत्ति या ब्रह्मा से उत्पत्ति आदी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण बात यह जानना है कि जब उन्होंने बुद्ध के रूप में सिखाना शुरू किया तब वैदिक दर्शन और उसके अभ्यासों के प्रति उनका दृष्टिकोण कैसा था? एक बार फिर बुद्धकाल में रचित बौद्ध ग्रंथ और बाद में लिखे गए वैदिक स्रोत हमें राइस डेविड्स द्वारा किए गए दावों के विपरीत बताते हैं। बुद्ध ने वेद की सत्ता को पूर्णतया अस्वीकार किया और इसके अभ्यास से मोक्ष प्राप्ति में किसी भी तरह की मदद मिलने की बात पर असहमति जनाई।
कभी-कभी उनकी आलोचनाएँ आज के लोगों की कल्पना से भी अधिक कठोर होती थीं – तेविज्ज सुत्त और चंकी सुत्त जैसे सुत्तों में उन्होंने वैदिक अभ्यास का पालन करने वालों को “अंधों की एक कतार” कहा है। अन्य अवसरों में उन्होंने वैदिक अनुष्ठानों को निरर्थक बताया है। ऐसी कई प्रथाएं जिन्हें उन्होंने अस्वीकार किया या अपने विचार के अनुसार ढाला उनमें से एक उनके समय में वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार की गई पशु-बलि की प्रथा थी। इसके अलावा, उनकी सबसे बड़ी दार्शनिक आलोचना वैदिक शिक्षा में कूटस्थ और अपरिवर्तनशील सत्ता के खिलाफ थी जिसे “आत्मा” के रूप में जाना जाता है।
अपने कई प्रवचनों में, उन्होंने स्पष्ट रूप से इस तरह की कूटस्थ, अपरिवर्तनशील और स्वतन्त्र अस्तित्वयुक्त कही जाने वाली “आत्मा” को न केवल अस्वीकार किया है बल्कि उसका खण्डन समेत किया है। अपने मूल उपदेश याने प्रतीत्यसमुत्पाद के सिद्धान्त पर आधारित “अनात्मा” की व्याख्या की। इसके आधार पर हम समझ सकते है कि बुद्ध ने वैदिक प्रणाली के कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड दोनों को अस्वीकार किया।
बुद्ध द्वारा दी गई ऐसी आलोचना के आधार पर ही वैदिक प्रणाली ने उनकी शिक्षाओं को “नास्तिक” धर्म कहा है । इसी प्रकार से षड्दर्शन के गुरुओं ने उनके द्वारा प्रतिपादन की गई “अनात्मा” की शिक्षा का खंडन करने का प्रयास किया। यहां पर हमें यह देखना है कि वैदिक प्रणाली सम्बन्धी बुद्ध द्वारा की गई आलोचना केवल षड्दर्शन के बीच में रहे कुछ अलग विचारों, या वेदों की विरोधाभासपूर्ण शिक्षा सम्बन्धी स्पष्टिकरण तक सीमित न होकर यह (आलोचना) समग्र वैदिक प्रणाली की शिक्षा के प्रति है। इस प्रकार प्रामाणिक बौद्ध परंपराओं ने हमेशा बुद्ध के मत वा सिद्धान्त को समझा है।
इसलिए यह सिर्फ एक गलत धारणा है कि बुद्ध जन्म से हिन्दु थे और मृत्यु के समय भी हिन्दू बने रहे ।