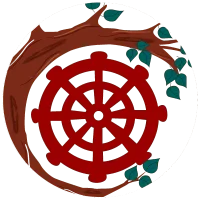- क्या आपने कभी पढ़ा या जाना है कि कैसे पारंपरिक बौद्ध और उनके ग्रंथों /आगमों ने बुद्ध और बौद्ध धर्म को परिभाषित किया है?
- क्या आप जानते हैं कि बौद्धों द्वारा संरक्षित प्रामाणिक बौद्ध ग्रंथों में क्या लिखा है?
- क्या आपने किसी शुद्धसिद्ध अटुट बौद्ध परम्परा के बौद्ध गुरु से बातचीत की है?
- क्या आपने कभी जाँचा है कि आपके बौद्ध धर्म के ज्ञान का स्रोत एक प्रामाणिक बौद्ध स्रोत है या गैर-बौद्ध वैदिक-हिन्दू?
ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें नेपाल और भारत के लोग बुद्ध या बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करते समय अक्सर अनदेखा कर देते हैं। वर्तमान समय में नेपाल और भारत में लोगों को विश्वसनीय बौद्धों द्वारा लिखित प्रामाणिक चिजें कुछ भी पढ़ने का अवसर शायद ही कभी मिलता है क्योंकि अक्सर लेख, किताबें, पत्रिकाएं और अन्य इंटरनेट के स्रोत इत्यादि में पाई जाने वाले सामग्रियां ऐसे विचारों से भरी होती हैं जिससे असली बौद्धधर्माभ्यासी अपरिचित हैं और जो बौद्ध धर्मग्रंथों में भी नहीं पाई जाती हैं। १२वीं शताब्दी के आसपास भारत में बौद्ध धर्म के पतन के बाद से प्रामाणिक और परम्परागत बौद्ध अवधारणाएँ भी जनसमूह में घटने लगीं। वैदिक हिंदू आचार्यों द्वारा बौद्ध धर्म की जानकारी और व्याख्याएं दी जाने लगीं जिसमें अक्सर बौद्ध सिद्धांतों और प्रथाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। अभी आप बौद्ध धर्म और बुद्ध के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, वह संभवत: उन्हीं स्रोतों से आया होगा। नीचे हमने बौद्ध परंपरा, इसके प्रसारण का इतिहास और नेपाल और भारत में इसकी वर्तमान स्थिति का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया है।
प्राचीन भारतवर्ष में “श्रमण” परंपरा नामक एक अलग आध्यात्मिक धारा थी जो वैदिक धारा के दायरे से बाहर थी। इस श्रमण परम्परा के अन्तर्गत बुद्ध और उनके शिष्यों ने वेदों को चौथे पुरुषार्थ अर्थात् मोक्ष प्राप्ति के हेतु प्रमाण के रूपमे कभी भी स्वीकार नहीं किया। बुद्ध और उनके अटुट परम्परा के शिष्यों ने वेदों में लिखी बातों, इसकी सहायक परंपराओं के साथ ही साथ अन्य समकालीन श्रमण आध्यात्मिक आंदोलनों जैसे जैन, चार्वाक आदि का खंडन किया। बुद्ध ने एक विशिष्ट दर्शन प्रणाली स्थापित की जिसे बाद में “बुद्ध-धर्म” अर्थात् बुद्ध या बुद्धों द्वारा प्रतिपादित धर्म (बौद्ध दर्शन) कहा गया। “अनात्मवाद” के नाम से प्रसिद्ध यह ज्ञान बुद्ध के बाद उनके शिष्यों में हस्तांतरित होता जाता है। अतीत के बुद्धों के उपदेश इस लोक से लोप हो जाने पर यही शिष्य बदले में बुद्ध बन जाते हैं और उन्हीं समान शिक्षाओं को सिखाने के लिए दुनिया में प्रकट होते हैं । बौद्ध ग्रंथ इस संबंध में दो बातें कहते हैं: प्रथम, बुद्धों की ऐसी परम्परा अटुट रुप में अनादी काल से चली आ रही है और द्वितीय, गंगा नदी में जितने रेत के दाने थे, उतनी ही संख्या में अतीत के बुद्ध थे और भविष्य में भी उतनी ही मात्रा में बुद्ध होंगे। वैदिक हिंदू धर्म ज्ञान की इस निर्बाध परंपरा के दायरे से बाहर है।
‘प्रतीत्यसमुत्पाद’( हेतुफल) का सिद्धांत सम्पूर्ण बुद्धोपदेशों का सार है जो वैदिक हिन्दु परम्परा में महत्त्वपूर्ण माने जाने वाले ‘आत्मा/ब्रह्म’, ‘सृष्टिकर्ता (ईश्वर)’, ‘प्रथम कारण’, ‘सांख्य दर्शन अनुसार के पुरुष तत्त्व’ या शिव, विष्णु जैसे देवताओं की शिक्षाओं आदि जैसे दार्शनिक मतों का खण्डन करता है । वे सभी चीजें जिन्हें “अस्तित्व” कहा जा सकता है, प्रतीत्यसमुत्पाद के सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं । इस हद तक कि इसके दायरे में ना पड़ने वाली विषयवस्तुओं का किसी भी स्थान या समय में अस्तित्व में होना संभव ही नहीं है। यही बौद्ध धर्म में सर्वोच्च सत्य है। इस दृष्टिकोण के आधार पर हमारे अस्तित्व की वास्तविकता पर वैदिक-हिंदू दार्शनिक सिद्धांतों को मिथ्यादृष्टि माना जाता है। इस प्रकार की मिथ्यादृष्टि को बौद्ध धर्म में दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है – शाश्वत्वाद और उच्छेदवाद । बौद्ध मानते हैं कि इस तरह की दृष्टियाँ सत्य के अनुसार नहीं हैं और ये सत्य अर्थात ‘यथाभूत ज्ञान दर्शन’ का साक्षात्कार करने के लिए सहयोगी नहीं हो सकते हैं। इसलिए हेतुफल सिद्धान्त और प्रतीत्यसमुत्पाद के इन सिद्धांतों के आधार पर बौद्ध धर्म ने अस्तित्व के सत्य से सम्बंधित वास्तविकता के बारे में अपना दृष्टिकोण स्थापित किया है जिसे ‘मध्यम प्रतिपदा’ कहते हैं । चूंकि केवल सत्य जैसा है, उसे वैसे ही रूप में देखकर (अर्थात् ‘यथाभूत ज्ञान दर्शन’ के माध्यम से) ही व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है इसलिए बौद्ध धर्म में यह माना जाता है कि अन्य सभी वैदिक-हिंदू दर्शन त्रुटियों से युक्त हैं और ये हमारे अस्तित्व की वास्तविकता को सटीक (सही )रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं । अपनी इस बात को प्रतिपादित करने के लिए वेद, पूर्व/उत्तर मिमांस (वेदान्त), सांख्य-योग, न्याय-वैशेषिक आदि जैसे वैदिक-हिन्दु मत के शाखाओं का खंडन करने के उद्देश्य से बौद्ध ग्रन्थराशि की रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। इसके बदले में इन गैर-बौद्ध दर्शनौं ने अपने स्वयं के दार्शनिक मान्यताओं की रक्षा के वास्ते बौद्ध विचारों का खंडन करने का भी प्रयास किया है। इसीलिए ये ऐतिहासिक दस्तावेज, बौद्ध और गैर-बौद्ध दर्शनौं के बीच हुए खंडन का आदान-प्रदान आज भी प्रमाण के रूप में उपलब्ध हैं जो इस तथ्य को प्रदर्शित करते हैं कि बुद्ध धर्म प्राचीन भारत में एक पृथक और विशिष्ट परंपरा थी।
हालाँकि, वैदिक हिंदू नेताओं और राजाओं द्वारा उत्पीड़न और दमन ने बौद्ध धर्म को कमजोर करना शुरू कर दिया, और १२वीं शताब्दी के आसपास जब नालंदा, विक्रमशिला, सोमपुरी, ओदंतपुरी आदि जैसे विशाल बौद्ध विश्वविद्यालय हमलावर इस्लामी ताकतों द्वारा नष्ट किये गए, बौद्ध धर्म अपने पतन के बाद अपनी रक्षा न कर सका । अंततः भारतवर्ष के मुख्य भूभागों में इसके विशिष्ट मार्ग और शिक्षाएं क्रमशः विकृत और क्षीण होती चली गईं । हालाँकि बौद्ध विचार भारत और इसके सांस्कृतिक क्षेत्रों में दो प्रमुख तरीकों से जीवित रहे: पहला तरीका कि यह वैदिक-हिंदू परंपराओं के विकास के लिए एक प्रेरणा बन गया जो भारतीय उप-महाद्वीप में फलता-फूलता रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि वैदिक-हिंदू परंपराओं ने कुछ बौद्ध शिक्षाओं को अपनी विचारधाराओं और प्रथाओं में समाहित कर लिया। यह क्रम पहले पौराणिक काल के दौरान से ही शुरू हो गया था जब बौद्ध धर्म के प्रभाव को कम करने के लिए बुद्ध को भी रणनीतिस्वरुप वैदिक तह में शामिल करने के लिए उन्हें विष्णु के अवतार के रूप में समावेश किया गया था। दूसरा तरीका यह कि बौद्ध शिक्षाओं की निरन्तरता भारतीय उपमहाद्वीप के बाहरी इलाकों जैसे काठमांडू, सिक्किम, भूटान, लद्दाख, बांग्लादेश की घाटी में कायम रही जहां इस्लामी हमलों का प्रभाव कम था।
सौभाग्यवश भारतवर्ष की मुख्य भूमि से लुप्त होने से पहले बुद्धधर्म अन्य पड़ोसी एशियाई देशों जैसे नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका, चीन में फैल गया था जहाँ इसने अपनी जीवित परंपरा को बनाए रखना जारी रखा। कहने का तात्पर्य यह है कि बौद्ध धर्म अपने ग्रंथों, साधना-निर्देशिकाओं , मौखिक शिक्षाओं (जो अभी भी सीधे शिक्षक से शिष्य को प्रेषित होती हैं )और पूजाविधियों आदि के आधार पर फलता-फूलता रहा जो भारत से इन देशों में रहने वाले शिक्षकों/विद्वानों द्वारा प्रसारित की गईं थीं । भारतवर्ष के बाहर बौद्ध धर्म तीन मुख्य वाहिनी द्वारा प्रसारित हुआ: प्रथम श्रावकयान का एक निकाय जिसे अब थेरवाद कहा जाता है, उसे तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में राजा अशोक के जेष्ट पुत्र ने श्रीलंका में प्रसारित किया । द्वितीय प्रमुख प्रसारण सहस्राब्दी की शुरुआत के आसपास भारतवर्ष के उत्तर-पश्चिमी भूभाग से होते हुए रेशम मार्ग के माध्यम से चीन में चला गया । तृतीय प्रमुख प्रसारण 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास नालंदा आदि विश्वविद्यालय के गुरुओं के संरक्षकत्व में तिब्बत में आयोजित किया गया था। प्रत्येक मामले में मौजूदा बौद्ध ग्रंथ जो विभिन्न उत्तर भारतीय भाषाओं जैसे प्राकृत या संस्कृत में थे, उनका अनुवाद दक्ष बौद्ध पंडितों और अभ्यासियों द्वारा पाली, चीनी और तिब्बती भाषा में किया गया । उनका यह परिश्रम सराहनीय है जिसके फलस्वरूप बौद्ध धर्म भारतवर्ष के मुख्य भूभाग के बाहर अच्छी तरह से संरक्षित रह सका । उन्होंने शाक्यमुनि बुद्ध से अटुट रुप में चली आई अभ्यास परम्परा को भी कायम रखा।
बौद्ध आगम तथा अधिगम के बारे में: बुद्ध के समय से बौद्धों ने सावधानीपूर्वक अपने स्वयं के ग्रन्थौं को कायम रखा है। उन्होंने 2500 वर्षों के भीतर अपने धर्मग्रंथों के कई विभिन्न संगायन अर्थात् संगीतियों का आयोजन किया है क्योंकि इन ग्रन्थौं की शुद्धता और इनमें आने वाली मलिनता बौद्धों के लिए विशेष प्राथमिक चिंता के विषय रहे हैं। हम जानते हैं कि श्रावकयान के एक निकाय थेरवाद ने अपने त्रिपिटक को संरक्षित करने के लिए आज तक छह संगायनो को आयोजित किया है । हस्तांतरित /प्रेषित होते आए इन ग्रंथों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है: पहला बुद्धवचन, जो बुद्ध के शब्द हैं जिन्हें सुत्त या सूत्र भी कहा जाता है । दूसरा बुद्ध के अपने शिष्यों और विगत शुद्ध/सिद्ध और अटुट जीवित परम्परा के गुरुओं द्वारा बुद्ध के उपदेशों को और ज्यादा स्पष्ट करने के लिए लिखी गईं टिप्पणियां जिन्हें टीका/भाष्य या शास्त्र कहते हैं। प्रारम्भ में ये आगम श्रुतिपरम्परा के द्वारा चल रहे थे और अंततः केवल इस्वी के शुरुआत के आसपास लिखने का काम शुरू हुआ । बौद्ध इन सूत्रों , शास्त्रों को अपनी शिक्षाओं का एकमात्र आधिकारिक स्रोत मानते हैं। किसी भी तथाकथित बौद्ध शिक्षाओं को इन ग्रन्थौं/शास्त्रों के अनुरूप होना जरुरी है । पारंपरिक बौद्ध ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार प्रारंभ में ये बौद्ध ग्रंथ चार प्रमुख भारतीय भाषाओं जैसे संस्कृत, प्राकृत, पैशाची और अपभ्रंश में लिखे गए थे। लेकिन विभिन्न कारणों से उनमें से अधिकांश ग्रन्थ भारतवर्ष के भूभाग से गायब हो गए । आधुनिक युग में भारतीय उपमहाद्वीप में केवल कुछ ही भाषाओं में लिखे गए ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं जो या तो पाली, बौद्ध वर्णशंकर संस्कृत जैसी प्राकृत भाषा या शास्त्रीय संस्कृत जैसी कुछ भाषाओँ में जीवित हैं। हाल ही में पाकिस्तान में कुछ नई पांडुलिपियां मिलीं जो गांधारी भाषा में लिखी गई थीं। अतीत में इन ग्रंथों /आगमों को अन्य मध्य एशियाई भाषाओं में भी लिखा गया था जिससे पता चलता है कि सिल्करोड के माध्यम से अन्य पड़ोसी देशों में बौद्धधर्म के प्रसारण के दौरान इन ग्रंथों /आगमों का ऐसी अनेकों भाषाओं में अनुवाद किया गया होगा।
इसी तरह “अनात्मा” का साक्षात्कार करने वाली ध्यान-पद्धती भी बुद्ध के समय से आज तक अविच्छिन्न रुप में गुरुशिष्य प्रणाली के माध्यम से शुद्धसिद्ध अटुट बौद्ध परम्परा चली आ रही है। इस तरीके की शुद्ध परम्परा से सिद्ध गुरु भी पैदा होते हैं। इसलिए एक प्रामाणिक बौद्ध परम्परा को दर्शाने के लिए एक अतिरिक्त विशेषण ‘सिद्ध’ भी जोड़ा जाता है। जो कोई भी इन दो आधिकारिक माध्यमों – ग्रन्थ/आगम तथा साधना परम्पराका से परे व्याख्या या कथित अनुभूति को प्राप्त करने का दावा करता है, उस व्यक्ति को एक प्रामाणिक बौद्ध परंपरा का गुरु नहीं माना जाता है। नेपाल और भारत के लोगों को इन जीवित बौद्ध परंपरा के बारे में पूरी तरह से जानकार नहीं है।
जागृत, बोधि प्राप्त किये हुए को बुद्ध कहतें हैं लेकिन यहाँ ‘जागृत’ वा ‘बोध’ भारतीय आध्यात्मिक इतिहास में पाए जाने वाले अन्य किसी भी प्रकार की जागृती या बोध को नहीं कहा गया है । बौद्ध बुद्ध के बोधि को अन्य परंपराओं से अलग करते हुए एक विशिष्ट तरीके से परिभाषित करते हैं। बुद्ध का बोधि अपने आप में ही एक बड़ा विषय है लेकिन इसे संक्षेप में इस तरीके से कहा जा सकता है: क्लेशावरण और ज्ञेयावरणको पूर्ण रुपसे हटानेवाले को बुद्ध कहा जाता है । पुद्गल नैरात्म्य और धर्म नैरात्म्यल को प्राप्त करने के परिणाम स्वरूप उस अवस्था में पहुँचा जाता है । इसके अलावा बुद्ध ने चार वैशारद्य, दशबल और अष्टादश आवेणिकधर्म के साथ साथ त्रिकाय अर्थात् धर्मकाय, संभोगकाय और निर्माणकाय को भी प्राप्त किया होता है। बुद्ध को चार प्रकार के मारों अर्थात् स्कन्धमार, मृत्युमार, क्लेशमार और देवपुत्रमार (जिन्होने सिद्धार्थ को बोधिज्ञान प्राप्त करने से रोकने की कोशिश की थी ) को हराने के दृष्टिकोण से भी समझाया जा सकता है। छह गुणों (भगों) के माध्यम से उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया जा सकता है। जिसकी वजह से बुद्ध को “भगवान’ भी कहा जाता है । ( यह ध्याiन देना जरूरी है कि बुद्ध को भारतीय आध्यात्मिक इतिहास में पहली बार ‘भगवान’ के नाम से सम्बोधित किया गया था) ये उपलब्धियां उन्हें तीन वा चार असंख्य कल्पों तक बोधिसत्त्वचर्या के परिणाम स्वरुप प्राप्त हुई थीं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इस बोधिसत्त्वचर्या के दौरान उन्होंने एकलाख पचास हजार सेअधिक बुद्धों से भेंट की। बुद्धोपदेशित मार्ग की अपनी ही विशेषताएं हैं जैसे बोधिचित्तोत्पाद, बोधिपाक्षिकधर्म, चतुरार्यसत्य, षट्पारमिता, समथा और विपश्यना का अभ्यास इत्यादि। इनमें से अधिकांश बातें भारतवर्ष के किसी अन्य गैर–बौद्ध परम्पराओं में न तो पाई जाती हैं और न ही सुनने को मिलती हैं। इन अवधारणों से मिलती जुलती बातें या तो बौद्ध विचारों / प्रथाओं का समावेश हैं या फिर संस्कृत भाषा की उसी प्रकार की शब्दावली के प्रयोग के कारण ये एक समान जैसी केवल दिखती मात्र हैं ।
इसके अलावा बुद्ध न तो सृष्टिकर्ता हैं और न ही कोई देवता या त्रिधातु (या त्रिभुवन)) में पाए जाने वाले किसी भी अन्य प्रकार के सत्त्वप्राणी। इसका अर्थ यह भी है कि वे मनुष्य भी नहीं थे। इन बातों को उन्होंने अपनी शिक्षाओं में बहुत स्पष्ट किया है। किसी को भी स्वयं को “बुद्धपुरुष” होने का दावा करने का अधिकार है लेकिन इस तरह का बोधि , बौद्ध ग्रंथों के वर्णन और बौद्ध ध्यान पद्धति के अनुसार “बुद्धता” के बराबर नहीं हो सकता। पूर्ण बुद्धता की लाभ प्राप्ति के लिए शुद्धसिद्ध और अटुट बौद्ध परम्परा के संग जुड़ना अनिवार्य है। इसके अलावा बौद्ध धर्मग्रंथों के उल्लेख अनुसार बुद्धों की ऐसी ज्ञानधारा की अटूट श्रृंखला तब तक जारी रहती है जब तक कि सभी सत्त्वप्राणी भविष्य में बुद्धत्व (बुद्धता) प्राप्त नहीं कर लेते। वैदिक-हिन्दु जैसे अन्य सभी धर्मसम्प्रदाय इस प्रकार के मार्ग और बोधिज्ञान की रेखा से बाहर है।
भारत और नेपाल में प्रचलित बौद्ध धर्म की भ्रांतियाँ और गलत व्याख्याएँ 2500 वर्षों के बौद्ध इतिहास, बौद्धों द्वारा सुरक्षित बौद्ध ग्रन्थराशि और बुद्ध के समय से अटूट रूप में चली आ रही अभ्यास परंपरा को सामान्यत: उपेक्षा करती हुई नज़र आती हैं । यह कहने की जरूरत न होगी कि इससे बढ़कर कोई और मिथ्या और भ्रामक बात क्या हो सकती है कि बुद्ध ने अपने ही विश्वसनीय और सिद्ध शिष्यों द्वारा यत्नपूर्वक संगृहीत ग्रंथों में उल्लेखित उपदेशों से हटकर कोई अन्य शिक्षा दी थी ।
इसलिए हम आशा करते हैं कि इस वेबसाईटकी की बातें बुद्धोपदेश के स्रोत के विषय से सम्बंधित भ्रांतियों को स्पष्ट करेंगी तांकि विशेष रूप से नेपाल और भारत के सदस्य इस अद्वितीय बौद्ध दृष्टिकोण, मार्ग और फल को समझ सकें जो वैदिक-हिंदू धर्म के किसी भी दर्शन से बिलकुल भिन्न है। वर्तमान समय में इसका बहुत अभाव रहा है। नेपाल और भारत में अधिकांश हिंदू और यहां तक कि कुछ बौद्ध, जिन्होंने अपनी वास्तविक जड़ें खो दी हैं, उन्होने भी अप्रामाणिक स्रोतों के आधार पर बुद्धधर्मसम्बन्धी ज्ञान को प्राप्त करते हुए केवल भ्रम की सृजना की है।
यह आपका व्यक्तिगत मामला है कि आप किस आध्यात्मिक परंपरा को चुनना चाहतें हैं। हालाँकि, यदि आप बौद्ध धर्म के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं तो आप सभी पाठकों और सब्सक्राइबरों से हम यह आग्रह करते हैं कि वे खुद से एक प्रश्न पूछें : “क्या मैं एक प्रामाणिक बौद्ध स्रोत से पढ़ रहा हूँ?”