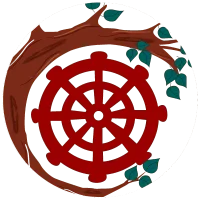बुद्ध के सम्बन्ध में यह भारत और नेपाल में सबसे बड़ी भ्रांतियों में से एक है। बौद्ध और वैदिक दोनों हिंदू ग्रंथ हमें एक अलग कहानी बताते हैं।
चूँकि श्रावकायन से लेकर महायान तक एक भी बौद्ध ग्रंथ ऐसा नहीं है जो इस विचार अर्थात् “बुद्ध विष्णु के अवतार हैं” की तरफ ज़रा भी इशारा करता या बढ़ावा देता हो इसीलिए जीवित बौद्ध परम्पराएं इस विचार से अनजान हैं। बौद्धों ने विष्णु को हमेशा कामधातु के देवताओं मध्य एक सामान्य देवता के रूप में लिया है। विभिन्न भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं द्वारा विष्णु को विभिन्न भूमिकाओं और शिक्षाओं के साथ प्रस्तुत किया गया है। बौद्ध दृष्टिकोण से यह कहना एक वहम है कि विष्णु “वैदिक देवता” हैं – ऐसी गलत बातें नेपाल और भारत में चली आ रही बुद्ध-अवतार संबंधी गलत अवधारणा की उत्पत्ति में योगदान देती हैं।
बौद्ध परंपरा में बुद्ध वे हैं जो अपने चित्तसन्तान के कर्मक्लेश के साथ साथ सम्पूर्ण अविद्या को निर्मूल कर त्रिभुवन या त्रिधातु के सभी प्रकार के भवबंधन को पार कर चुके हैं। उनके ज्ञान और शक्तियों को भी पूरे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके विपरीत विष्णु जैसे देवताओं को शक्तिशाली देवताओं के रूप में माने जाने के बावजूद भी वे बौद्ध परंपरा के अनुसार जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमने वाले केवल एक प्राणी ही हैं। वास्तव में भगवान विष्णु को महायान में “क्लेशों” के प्रतिनिधि के रूप में दर्शाया गया है। इसलिए बौद्ध धर्म में भगवान विष्णु की स्थिति निम्न कोटी की ही है । उनको सृष्टिकर्ता या कुछ वैदिक हिंदू भाष्यों में चित्रित किये अनुसार पूरी दुनिया का पालन करने वाले पालनहार, परमेश्वर का दर्जा नहीं दिया जाता है। ऋग्वेद में तो विष्णु को इंद्र से भी निम्न स्थान दिया गया है। वास्तव में उन्हें अक्सर बुद्ध के एक सामान्य शिष्य के रूप में बौद्ध धर्म में चित्रित किया गया है।
विभिन्न प्रकार के बौद्ध साहित्यों में विष्णु का उल्लेख बारम्बार किया गया है। दीघनिकाय के “महासमय-सुत्त” जैसे श्रावकयान के सुत्तों (सुत्रौं) में यह उल्लेख पाया जाता है कि विष्णु बुद्ध की वंदना करने के लिए आते हैं। इस सुत्त में दो बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं: बुद्ध की वंदना करने लिए आए तैंतीस देवताओं के मध्य विष्णु का दर्जा निम्न है और बुद्ध को स्पष्ट रूप से उन देवताओं से उच्च स्थान दिया गया है। संयुक्तनिकाय के “वेण्डुसुत्त” में “बुद्ध की वन्दना करने वाले सुखी रहते हैं” यह कहते हुए विष्णु द्वारा बुद्धका स्तुतिगान किया गया प्रसंग उल्लेखित हैं । अभिधर्म के रूप में माने जाने वाले अर्थविनिष्कयसूत्र में बुद्ध के शरीर में ३३ वां महापुरुष-लक्षण था जो कि महानारायण- शरीर की तरह ही हर तरफ से रमणीय था । (नारायण विष्णु का दूसरा नाम है) तथागतों की मूर्तियों का निर्माण, टूटे हुए बौद्ध स्तूपों की मरम्मत और पिछले जन्मों में डरे हुए लोगों को सांत्वना देना (बौद्ध धर्म में एक प्रकार का दान (भेंट) माना जाने वाला मनोवैज्ञानिक सांत्वना है) इस तरह के निशान को प्राप्त करने के कारणों के रूप में समझाया गया है। धर्मवर्द्धनसूत्र, ललितविस्तरसूत्र, अक्षयमतिनिर्देशसूत्र, महापरिनिर्वाणसूत्र, श्रीमहादेवीव्याकरणसूत्र, कारण्डव्यूहसूत्र, लंकावतारसूत्र, अनित्यतासूत्र, दशभूमिकसूत्र, विमलकीर्तिनिर्देशसूत्र, रत्नकेतुपरिवर्तसूत्र, सद्धर्मपुण्डरिक, नारायणपरिपृच्छासूत्र जैसे कई महायान सूत्रों में बुद्ध विष्णु (नारायण), ब्रह्मा, वरुण, सक्र (इन्द्र) आदि देवताओं से घेरे हुए पाए जाते हैं । इनमें से अधिकांश सूत्रों में विष्णु को न केवल बुद्ध के शिष्य के रूप में अपितु उन्हें ब्रह्मा और शक्र (इन्द्र) की तुलना में न्यून भूमिका में पाया जाता है। उदाहरण के लिए ललितविस्तर सूत्र में यह उल्लेखित है कि नारायण ने भी सभी प्रमुख देवताओं के साथ मिलकर बुद्ध का चरणस्पर्श किया । हालांकि उदाहरण के तौर पर अन्य सूत्र जैसे अक्षयमतिनिर्देशसूत्र में एक दिलचस्प बात पाई जाती है कि बुद्ध ने दम्भी, घमण्डी, उग्र और क्रोधी प्राणियों को वश में करने के लिए नारायण, इन्द्र, ब्रह्मा, लोकपाल आदि जैसे देवताओं के बराबर ही शक्ति का प्रदर्शन किया । इस संदर्भ में नारायण की शक्ति की तुलना बुद्ध की शक्ति का मापन करने वाली एक इकाई के रूपमे चित्रित की गई है जो आजकल इंजनों की शक्ति का नापन करने के लिये ‘हर्सपावर’ का उपयोग करने के बराबर है। वसुबंधु (चौथी-पांचवीं ईस्वी) द्वारा रचित अभिधर्मकोषभाष्य में बुद्ध की शक्ति का मापन करने के लिए विष्णु की शक्ति अर्थात् नारायण इकाई के उपयोग का विस्तृत वर्णन पाया जाता है। इसमें ऐसा कहा गया है कि एक नारायण इकाई करीब दस लाख साधारण हातियों के बल के बराबर होती है । वसुबंधु ने बुद्ध में असंख्य नारायण इकाई बराबर की शक्ति का उल्लेख करते हुए इस विषय पर व्याख्याओं का अंत किया है।
इसके अतिरिक्त कारण्डव्यूहसूत्र में शिव, विष्णु (नारायण) आदि जैसे देवताओं के संबंध में एक और दिलचस्प बौद्ध अवधारणा का पता चलता है। उसमें उल्लेखित है कि नारायण की उत्पत्ति बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के हृदय से हुई थी । इसके अलावा इस सूत्र में कहा गया है कि जो प्राणी नारायण को बहुत पसंद करते थे उन प्राणियों को अवलोकितेश्वर, नारायण के स्वरूप में प्रकट होकर शिक्षा दे सकते थे। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि बोधिसत्व अवलोकितेश्वर दशभूमि अर्थात् पूर्ण बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए केवल एक कदम पिछे की दूरी में पहुंचे हुए बोधिसत्त्व हैं । उनका ज्ञान अभी भी पूर्ण बुद्धत्व प्राप्त किये हुए शाक्यमुनि के ज्ञानस्तर से निम्न ही माना जाता है । यह तुलना एक बार फिर बौद्ध धर्म में विष्णु की स्थिति को दर्शाती है (कि वो अवलोकितेश्वर से भी ज्ञान और शक्तिमे निम्न है तो बुद्ध से उनकी क्या तुलना हो सकती है?)। पुनः नारायण परिपुच्छ सूत्र जैसे कुछ महायानसूत्रों में विष्णु को एक वार्ताकार के रूपमें चित्रित किया गया है जहाँ वे एक साधारण शिष्य के रूपमे बुद्ध से प्रश्न करते हैं। ऐसे महायान सूत्रों में नारायण या विष्णु को बुद्धत्व प्राप्ति के लिए बुद्धपथ का अनुसरण करने वाले बोधिसत्त्व के रूपमें दिखाया गया है। श्रीलंका की थेरवाद परंपरा में विष्णु को बुद्ध द्वारा नियुक्त धर्मपाल माना जाता है।। वहां उन्हें उप्पलवण्ण अर्थात् “नीले रंग” का देवता के नाम से पुकारा जाता है। विष्णु का यह विवरण वैदिक हिन्दु ग्रन्थ में उल्लेखित विवरण से मिलता है और बौद्ध ग्रंथों जैसे योगाचारभूमि में पाए जाने वाले विष्णु की विशेषताओं के अनुरूप है जिसमें उन्हें तीन चेहरे, हरा-पीला रंग, दाहिने हाथ में सुदर्शन-चक्र और गरुण नामक एक पौराणिक पक्षी पर सवारी किये हुए के रूप में वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त वज्रयान परंपरा में वह ‘मंडल’ में एक संरक्षक देवता के रूप में प्रकट होते हैं जो मुख्य बौद्ध ईष्ट-देवता के साथ-साथ बुद्ध और बोधिसत्वों के अधीनस्थ होते हैं । अत: इन सभी प्रमाणों और कारणों के आधार पर विष्णु के संबंध में बौद्धों की परिचितता और बौद्ध ग्रंथों में उनकी उपस्थिति को देखते हुए, विष्णुकी तुलना बुद्ध से करना या उन्हें वैदिक देवता कहना आश्चर्यजनक है। बौद्ध धर्म में उनकी बहुत छोटी भूमिका है और वास्तव में उन्हें अक्सर बुद्ध के एक सामान्य शिष्य के रूप में चित्रित किया जाता है।
इस विषय में स्वयं बुद्ध का कथन और भी महत्वपूर्ण है। दोणसुत्त (द्रोणसूत्र) में दोण नामक एक ब्राह्मण से किये वार्तालाप में बुद्ध ने स्वयं को किसी भी देवता होने से इनकार करते हुए कहा है कि उन्हें केवल ‘बुद्ध’ के नाम से जाना जाए। यहां बुद्ध की तुलना पूरी तरह से खिले हुए कमल से की गई है जो पूरी तरह से संसार के मलसे उठे हैं और इस प्रकार संसार में पाए जाने वाले छह श्रेणियों के प्राणियों से परे हैं। बुद्ध का ऐसा चित्रण बौद्ध ग्रंथों में काफी सामान्य है।
इसके अतिरिक्त हम वैदिक हिंदू साहित्यों में वर्णित विष्णु के अवतार के रूप में बुद्ध और बौद्ध ग्रंथों में वर्णित शाक्यमुनि बुद्ध के बीच तथ्यात्मक भिन्ताएं पाते हैं। इस्वी की पहली शताब्दी के लगभग आरम्भ से पुराणों की रचना शुरू होने के साथ साथ विष्णु एक महत्वपूर्ण देवता के रूप में प्रकट होने लगते हैं । उस युग के पुराण ग्रंथों की श्रृंखला जैसे हरिवंश, विष्णु पुराण (3.17.18), भागवत पुराण (1.3.24, 2.7.37, 11.4.23), गरुड़ पुराण (1.1, 2.30.37, 3.15) 26), अग्नि पुराण (अध्याय 16, ‘बुद्धाद्यवतारकथन’), नारद पुराण (2.72), लिंग पुराण (2.71), पद्म पुराण (3.252) आदि में हम चार मुख्य भिन्नताएं पाते हैं:
१) बुद्ध की माता का नाम: बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध की माता का नाम मायादेवी है लेकिन बुद्धावतार विष्णु की माता का नाम अंजना है।
२) बुद्ध का जन्मस्थल: शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था लेकिन बुद्धावतार विष्णु का जन्म किकट में हुआ था।
३) बुद्ध की देशना और उनकी गतिविधियां: पुराणों के अनुसार वेद की भर्त्सना करने वाले असुरों को भ्रमित करने के लिए विष्णु ने अपना सबसे निकृष्ट (बुरा ) मायामोह का स्वरुप बुद्ध के रूप में प्रकट होकर दिखाया। लेकिन बुद्ध ने तो विशिष्ट प्रकार का धर्म सिखाया था जो न तो किसी असुरोंके प्रति लक्षित था और न ही इसने किसी हिंसा, घृणा या मोह जैसे क्लेश को ही बढ़ावा देता है । जबकि हम पाते हैं कि मनुष्य, देवता और अनगिनत अमनुष्य सभी उतनी ही रूचि और वीर्यपूर्वक बुद्धोपदेश सुनते थे । शीलाचरण के दृष्टिकोण से बुद्ध की शिक्षा त्रुटिहीन हैं। उनके द्वारा दी गई शिक्षा सर्वव्यापक प्रेम, सद्भाव और सुख की वृद्धि करती है। असुरों को मोहित करने के लिये विष्णुका स्वरुप अवतरित होने का जिक्र करने वाली यह पौराणिक कथा तो क्षेमेन्द्र, दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द, सर्वपल्ली राधाकृष्णन आदि जैसे बहुत से वैदिक हिन्दु गुरुओं के कथन के विरुद्ध होगी जिन्हौंने बुद्ध के उपदेशों को भारतीय अध्यात्मवाद में सर्वोत्कृष्ट माना है । वहीं दूसरी ओर वैदिक साहित्य में बुद्धावतार विष्णु का कोई भी उपदेश नहीं मिलता है । ऐसी काल्पनिक कथाओं के अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है ।
४) बुद्ध के प्रकट होने का समय – बुद्ध और बुद्धावतार विष्णु के प्रकट होने का कालखण्ड भी मेल नहीं खाता । वैदिक बुद्ध कलियुग की शुरुआत में आने वाले थे। तीन युगों के संबंध में लोकप्रिय गणनाओं के अनुसार यह अक्सर कहा जाता है कि कलियुग लगभग ३१०० ईसा पूर्व शुरू हुआ था; हालाँकि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म ५०० ईसा पूर्व के आसपास हुआ था।
इसलिए कुछ सतही समानता जैसे “बुद्ध” नाम के अलावा इन ग्रंथों में बुद्ध के रूप में विष्णु के अवतार का हमारे समय के शाक्यमुनि बुद्ध से कोई लेना-देना नहीं है। अद्वैत वेदान्त आदि जैसे वैदिक हिन्दू परम्पराओं में बुद्ध को किसी का भी अवतार नहीं कहा गया है।
प्राचीन भारतवर्ष में वैदिक शास्त्र में भी पारंगत बौद्ध गुरुओं ने विष्णु के बारे में पूरी तरह से अलग ही अवधारणाओं की प्रस्तुति की है। भारतवर्ष में कनिष्क (इस्वी के लगभग पहली शताब्दी ) के काल में प्रख्यात एक महायानी बौद्ध गुरु शंकरस्वामी ने ‘देवतास्तव’ नामक अपने काव्य में उल्लेख किया है कि बुद्धको उनके सद्गुण के कारण वैदिक साहित्य में भी स्वीकार किया गया है । हालाँकि उल्लेखनीय बात यह है कि उन्होंने अपने लेख में शाक्यमुनि बुद्ध और विष्णु को अलग व्यक्तित्व के रूप से प्रस्तुत किया है। उदाहरण के लिए, वह कहते हैं कि बुद्ध न तो उन लोगों का पक्ष लेते हैं जो उन्हें उच्च सम्मान देते हैं और न ही उन लोगों को नापसंद करते हैं जो उन्हें विरोधी के रूप से देखते हैं; जबकि शिव, विष्णु आदि देवता उनका विरोध करने वाले प्राणियों को दंडित करते हुए अपने अनुयायियों को वरदान देते हैं। इसका कारण यह है कि बुद्ध के विपरीत वे क्लेशों से मुक्त नहीं हैं, लेकिन बुद्ध किसी भी क्लेश से दूषित नहीं हैं और उन प्राणियों की गतिविधियों की परवाह किए बिना हमेशा प्राणियों के प्रति करुणा का भाव बनाए रखते हैं।
इसके बाद किसी भी बौद्ध साहित्य में या किसी भी लेखक ने विष्णु को अवतार की कथा के साथ जोड़कर प्रस्तुत नहीं किया है। आचार्य यशोमित्र (छठी शताब्दी) ने एक बार फिर विष्णु को अपने ग्रंथ ‘अभिधर्मकोशव्याख्या’ में उद्धृत करते हुए उल्लेख किया है कि विष्णु का ‘विराट रुप’ जैसा चमत्कार प्राणियों को सांसारिक प्रपञ्च से मुक्त नहीं करता है। जबकि इसके विपरीत बुद्ध ने संसार रुपी भवसागर को पार करने के लिए सद्धर्म रुपी हात देकर सत्य का साक्षात्कार कराने वाले त्रुटिरहित धर्म को सिखाया है । आचार्य धर्मकीर्ति (7वीं शताब्दी) ने “सुभाषितरत्नकोश” में एक व्यंग्यात्मक श्लोक लिखा है कि लोग बुद्ध पर झूठ का आरोप लगाते हैं भले ही वे सच क्यों ना बोल रहे हों लेकिन कवि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण की कहानी को ऐसे लोग सच मान लेते हैं। उन्होंने यहां संकेत दिया है कि विष्णु, राम आदि के तथाकथित अवतार की कहानी एक सच्ची कहानी नहीं है। एक अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध लेखक आचार्य चंद्रकीर्ति ने अपनी मौलिक रचना “मध्यमकावतार” में कहा है कि वैदिक साहित्य में उल्लेखित “ईश्वर,” “प्रकृति,” “पुरुष” वा “नारायण” से सृष्टि की रचना नहीं हुई है। गहरे दार्शनिक निहितार्थ के अलावा, उनका यह विचार पौराणिक विचार का खंडन करता है कि नारायण ने ही संसार की सृष्टि की है। तिब्बत में बौद्ध धर्म की स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख शान्तरक्षित (आठौँ शताब्दी) ने अपनी उत्कृष्ट रचना ‘तत्त्वसंग्रह’ में वैदिक-हिंदू परंपराओं की सभी शाखाओं का व्यापक खंडन किया है। वैदिक-हिंदू परंपरा के बारे में उनकी समझ बुद्ध और अन्य बौद्ध विद्वानों के अनुरूप है। ऐसी बौद्ध अवधारणाएं बुद्ध की सर्वोच्चता के साथ साथ शाक्यमुनी बुद्ध और पुराणों में उल्लेखित बुद्धावतार विष्णु की भिन्नता की भी पुष्टि करते हैं जिसे न केवल समकालीन बौद्धों अपितु प्राचीन भारतवर्ष के सिद्ध आचार्यों ने भी समर्थन किया है।
अतः हम कह सकते हैं कि:
i) प्राचीन भारतवर्ष में पौराणिक ग्रंथों में पाए जाने वाले विष्णु की अवधारणा और शाक्यमुनि बुद्ध को बौद्ध समान रूप में नहीं देखते थे क्योंकि इन दोनों के बीच के भेद से वे अच्छी तरह वाकिफ थे।
ii) तत्कालीन भारतवर्ष के समाज में “बुद्ध विष्णु के अवतार हैं” जैसी अवधारणाएं उतने प्रमुख नहीं थीं जितनी आज हम पाते हैं।
iii) बौद्ध धर्म में विष्णु को हमेशा एक साधारण देवता के रूप में लिया गया था।
बुद्धावतार विष्णु का विचार भारत में कब से आम जनता पर हावी हो गया? ऐसा प्रतीत होता है कि यह धारणा ११वीं -१२ वीं शताब्दी के आसपास वैष्णव संप्रदायों द्वारा और आगे बढ़ाया गया। “गीतगोविन्द” में लेखक जयदेव और काश्मिरी बहुज्ञ क्षेमेन्द्र ने अपने “दशावतारचरित” में बुद्ध की कथा को काल्पनिक कहानियों के साथ जोड़ते हुए बुद्ध को विष्णु के अवतार के रूप में बताने का पुनः प्रयास किया।
ये दोनों काव्य रचनाएँ थीं जो साहित्यिक रूपक और कल्पना से भरी पढ़ी हैं। परन्तु इनमें लिखी घटनाओं का न तो विवरण और न ही उनका वर्णन बौद्ध ग्रंथों में पाए जाने वाली बुद्ध की जीवनी और शिक्षाओं के साथ पूरी तरह से मेल खाता है । इसके अलावा १४वीं शताब्दी के प्रभावशाली वेदांतिक शिक्षकों में से एक माधवाचार्य ने एक बार फिर से पौराणिक कल्पित कथा को दोहराया जिसमें कहा गया है कि विष्णु ने ‘बुद्ध’ नामक एक बालक का रूप धारण कर असुरों को मोहजाल में बहकानेका काम किया । वैदिक ग्रंथों में पाई जाने वाली ऐसी कहानियाँ वैदिक बुद्धावतार विष्णु और उनकी शिक्षाओं के बारे में गंभीर संदेह पैदा करती है। और इस तरह के मिथकों और प्रचारों का शाक्यमुनि बुद्ध से कदापि कोई संबंध नहीं है। इस तरह की विसंगतियों को ठीक से महसूस करते हुए आज के समकालीन वैदिक गुरु जैसे गोवर्द्धन पीठ के शंकराचार्य तथा स्वामी निश्चलानंद सरस्वती स्वीकार करते हैं कि वैदिक साहित्यों में वर्णित विष्णु के अवतार बुद्ध और बौद्ध धर्म के शाक्यमुनि बुद्ध दो अलग-अलग व्यक्तित्व हैं। कुछ समय पहले विपश्यनाचार्य स्वर्गीय सत्यनारायण गोयन्का ने काँची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जयेन्द्र सरस्वती को भी इस विषय में सहमत करवाकर विगत में इस प्रकार की त्रुटियाँ हुई हैं ऐसा एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी करवाई ।
इसके अतिरिक्त यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि श्रुति (अतीत में द्रष्टा-ऋषि द्वारा बिना किसी मध्यस्थता के सुना गया, इसलिए इसे अपौरुषेय कहा गया है – जैसे कि चार वेद) की तुलना में स्मृति को (मनुष्यों द्वारा मध्यस्थ – कुछ ऋषि- मुनियों द्वारा याद कर संगृहीत की गईं जिसके कारण इसमें त्रुटि होने की संभावना हो सकती है – जैसे पुराण) वैदिक परंपरामे समान रुपसे आधिकारिक नहीं माना जाता है। इसलिए वैदिक हिंदू धर्म की मान्यतानुसार भी पुराणों के कथनों पर भी प्रश्न वा उनका खण्डन किया जा सकता है। वास्तव में पौराणिक कथाएं तथा उनके भीतर की शिक्षाएँ कईं अवसरों पर एक आपस में विरोधाभासी हैं जैसे बुद्ध को विष्णु के अवतार के रूप में वर्णन करना। स्वामी विवेकानंद का कहना है कि आधुनिक युग में तथाकथित हिन्दुधर्म की ज्यादातर बातें पौराणिक ग्रंथों से ली गईं हैं।
दशरथजातक में उल्लेखित रामपण्डित के प्रसंग को लेकर हाल के दिनों में हम अवतारसम्बन्धी एक और फैली हुई भ्रांति को देखते हैं। बुद्ध द्वारा सुनाई गई जातक कहानियां बौद्ध ग्रंथों का संग्रह हैं जो शाक्यमुनि बुद्ध के पिछले जीवन की कहानियों के बारे में सूचित करते हैं जिस समय वे सम्यकसम्बुद्ध बनने के लिए बोधिसत्व के रूप में प्रयास कर रहे थे। पाली स्रोतअनुसार इस जातकमें बुद्ध पहेले किसी जन्म में “रामपण्डित” के रुप में पैदा हुए थे और उन्होंने उस जन्म में “नैष्क्रम्य पारमिता” को पूरा किया था। यह अभ्यास सम्यकसम्बुद्ध प्राप्त करने के लिए अनिवार्य अंग है जो बुद्धोपदेश के अनुरूप है। हालाँकि इस जातक की अक्सर गलत व्याख्या का कारण इसके पात्रों के नाम और घटनाक्रम बाद के वैदिक ग्रंथों जैसे वाल्मीकि के ‘रामायण’ के साथ समानता के कारण हैं।
हिंदू धर्म के भीतर एक स्वीकृत मान्यता है कि वाल्मीकि त्रेता युग (एक पौराणिक समयरेखा) में थे। इसके अलावा यह कहने के लिए कोई ऐतिहासिक रूप से सिद्ध प्रमाण नहीं हैं कि वाल्मीकि रामायण जातक से पहले थे। इस जातक में रामपण्डित, लक्ष्मण और सीता भाई-बहन हैं और इसमें रावण जैसे पात्र और सीता के अपहरण की घटना भी नहीं है । संभवतः इस जातक कथा से वैदिक-हिंदू रामायण की कथा का मूल निकाला गया था जिसमे रामपण्डित को त्याग और धार्मिकता जैसे गुणों के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। यदि रामपण्डित ही विष्णु होते, तो कुछ अवांछित परिणाम होते:
क) विष्णु जन्म और मृत्यु के चक्र में रहने वाले एक साधारण प्राणी हैं जिस तरह से इस जातक कहानी में रामपण्डित ।
ख) या विष्णु बौद्ध धर्म के महायान अभ्यास कर रहे एक बोधिसत्त्व थे जिससे वैदिक साहित्य अनुसार उनका “सृष्टिकर्ता” वा “संसार के पालनहार” के रूप में परिचय असत्य ठहरता है।
इसलिए इस अवतार मिथक का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है।
बुद्ध ने खुद को इक्ष्वाकुवंशी बताया है । वैदिक राम को भी उसी वंश का माना जाता है। हालाँकि अगन्नसुत्त के आधार पर हम पहले ही बता चुके हैं कि मनुष्यों पर शासन करने वाले “प्रथम क्षत्रिय राजा” की अवधारणा के संबंध में बुद्ध का विचार वैदिक हिन्दू धर्मकी तुलना में किसी भी तरह से मेल नहीं खाता है। – बुद्ध जन्म से हिन्दू थे और मृत्यु के समय भी हिन्दू थे
इसके अलावा वाल्मीकि रामायण के कुछ विवरणों में अयोध्या कांड का एक श्लोक है जो तथागत (यानी बुद्ध) पर चोर होने का आरोप लगाता है। इससे यह पता चलता है कि वाल्मीकि रामायण की रचना बुद्ध के बाद हुई थी। वैसे भी रामायण के विभिन्न संस्करणों और रजिस्टरों पर काम करने वाले अधिकांश आधुनिक विद्वान इस बात से सहमत हैं कि वाल्मीकि रामायण की रचना बुद्ध के बहुत बाद में हुई थी।
वैदिक हिंदू धर्म में न तो बुद्ध की पूजा करने के लिए कोई वास्तविक साधना या विधि है और न ही बौद्ध ग्रंथों को इसके पारंपरिक साहित्य के संग्रह में शामिल किया गया है। बौद्ध भी अपने आधिकारिक सिद्धांतों के भीतर किसी भी वैदिक हिंदू ग्रंथ को शामिल नहीं करते हैं। वास्तव में वैदिक हिंदू पंडितों और विद्वानों को बुद्ध का अनुसरण करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है क्योंकि उन्हें विष्णु के सबसे बुरे रूप में चित्रित किया गया है जो उन राक्षसों (असुरों) को भ्रमित (मायामोहस्वरूप) करते हैं जो वेदों की सत्ता को अस्वीकार करते हैं। संभवतः यह प्रचार बौद्धों की ओर निर्देशित किया गया है। यह आदि शंकर की आत्मकथाओं से भी सिद्ध होता है जैसे कि माधवाचार्य द्वारा रचित शंकरदिग्विजय जिसमें यह बताया गया है कि बौद्धों को आदि शंकर और उनके अनुयायी, राजा सुधनवन के हाथों शारीरिक अत्याचारों का सामना करना पड़ा था।
बुद्ध को विष्णु का नौवां अवतार कहने के अलावा, पारंपरिक वैदिक हिंदू विद्वानों ने कभी भी बौद्ध ग्रंथों को अधिकारिक ग्रंथों के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। इसी तरह बुद्ध और बौद्ध लेखकों ने भी वैदिक हिंदू विद्वानों का खंडन करने या अपने स्वयं के दर्शन को सिखाने के अतिरिक्त किसी भी वैदिक हिंदू ग्रंथों को उद्धृत नहीं किया, न ही वे उन्हें कोई प्रामाणिक ज्ञान मानते हैं।।