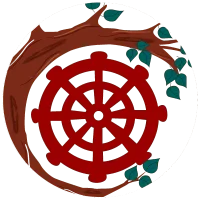वैशाख पूर्णिमा की सुबह बोधगया में बोधिवृक्ष के नीचे बुद्ध को बोध (एहसास) हुआ धर्म यही है । यह बौद्ध धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत है और यही इसे अन्य सभी धार्मिक प्रणालियों से अलग करता है। इसे संस्कृत में प्रतीत्यसमुत्पादऔर पाली में पटीच्चसमुप्पाद कहा जाता है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद अन्योन्याश्रित सह-उत्पत्ति / अन्योन्याश्रित सह-उत्पन्न या आश्रित-उत्पत्ति के रूप में किया जाता है।
यह बहुत आसान है, लेकिन इसकी सादगी के कारण, हमारे जटिल-अभिसंस्कृत मन को यह बहुत जटिल (कठिन)लगता है। इसका सीधा सा मतलब है कि सभी भौतिक या अमूर्त धर्म, हेतु-प्रत्ययों के जुटने के कारण उत्पन्न होते हैं और ये हेतु-प्रत्यय भी पहलेके अन्य हेतु-प्रत्ययों से होते हुए अनादि काल और अनंत काल तक जारी रहते हैं। जो कुछ भी प्रकट होता है, वह तब प्रकट होता है जब उचित हेतु-प्रत्यय मौजूद हों।
यह संसार हेतु-प्रत्ययों का एक अनादि परिवर्तनशील प्रवाह है जिसे संस्कृत में हेतु-फल प्रवाह कहा जाता है। पदार्थ या समय की सबसे छोटी इकाई से लेकर त्रिसहस्र महासहस्र लोकधातु , यह महायान और थेरवाद बौद्ध धर्म के लोकधातु (ब्रह्मांड) में पाई जाने वाली एक अवधारणा है जिसमें एक लोकधातु (ब्रह्मांड) तीन हजार लोक-प्राणालियों से मिलकर बनता है और प्रत्येक लोक-प्राणाली, हजारौं संसार (लोकों) से मिलकर बनती है, ऐसा कहा जाता है। सभी (चीज़ें ) हेतु -प्रत्ययों के माध्यम से उत्पन्न होती हैं (या सही मायनों में उत्पन्न होते हुए दिखती हैं)। यह (नियम)अवधारणाओं/ विचारों और अमूर्त वस्तुओं पर भी लागू होता है।
एक विशेष घर केवल ईंटों, मिट्टी, डिजाइन, लकड़ी, कांच, सीमेंट, टिन, टाइल, बढ़ई, राजमिस्त्री और इंजीनियरों आदि के संयोजन जैसे हेतु-प्रत्ययों का एक संग्रह मात्र है। लेकिन ये प्रत्येक हेतु-प्रत्यय भी उनके अपने हेतु-प्रत्यय आदि के कारण उत्पन्न होते हैं। यदि कोई ईंट या मिट्टी (हेतु आदि) या राजमिस्त्री आदि नहीं होते, तो घर नहीं उठता / प्रकट होता। लेकिन ईंट घर नहीं है, टिन या मिट्टी या सीमेंट या लकड़ी, कांचआदि भी घर नहीं हैं और यदि आप उन सभीको एक-एक करके निकालेंगे तो कोई घर भी नहीं होगा। इसलिए वह प्रतीत्यसमुत्पन्न (विभिन्न हेतु-प्रत्यय पर निर्भर होकर उत्पन्न हुआ ) घर वास्तविक अस्तित्वसे रहित है अर्थात् निःस्वभाव है। इस निःस्वभावता या अवास्तविक अस्तित्व-पन (अस्तित्व की अवास्तविकता) को बुद्ध धर्म में शून्यता कहतें हैं।
आप जहां पर बैठे हैं, आप उसे “यहाँ” कहतें हैं, लेकिन उसी स्थान को मैं “वहाँ” कहूंगा क्योंकि आपका ‘यहाँ’ आपके उस स्थान के होने पर निर्भर है और वही स्थान मेरे लिए “वहाँ” है जो मेरे उस जगह में न होने पर निर्भर करता है। इसलिए वास्तव में वह स्थान न तो “यहाँ” है और न ही “वहाँ” है। दूसरे शब्दों में, “यहाँ” या “वहाँ” के अस्तित्व का कोई वास्तविक अस्तित्व नही है । अर्थात् ये निस्वभाव या शून्य हैं। छोटा और लंबा, दूर और निकटआदि भी ऐसी ही धारणाएं हैं। आइन्स्टाइन के कहे अनुसार, वे सभी सापेक्षिक हैं। इस अवधारणा और इसके सभी अर्थों की व्याख्या करने में बहुत अधिक समय लगेगा और वैसे भी केवल लेखों या किताबों के माध्यम से यह पूर्ण रूप से समझा नहीं जा सकता। लेकिन संभवतः केवल एक प्रामाणिक गुरुसे चरणबद्ध रूपमें सीख कर इसको सही ढंग से समझा जा सकता है।
बौद्ध/बोधि का अर्थ शून्यता या प्रतीत्यसमुत्पाद का अविकल्प बोध है, इसे केवल अवधारणात्मक/विकल्पात्मक रूप से समझना संभव नहीं है। इस प्रकार, हमें उस बोध प्राप्ति के मार्ग पर मार्गदर्शन करने के लिए एक प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता होती है। यह क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें दुःख, क्लेश और कर्म से मुक्त करानेका वाला सम्यक् बोधि केवल लेख या किताबों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है ।
उस प्रत्यक्ष बोध के बिना, आप लोभ, अविद्या और अपने कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। पहली शताब्दी के महान ब्राह्मण बौद्ध गुरु नागार्जुनने अपनी उत्कृष्ट रचना, मध्यमकशास्त्र (मध्यमकशास्त्र (जिसे मूलमाध्यामाकारिका के नाम से जाना जाता है) में लिखा है:
कर्मक्लेशक्षयान् मोक्षः कर्मक्लेशा विकल्पतः ।
ते प्रपञ्चात् प्रपञ्चस् तु शून्यतायां निरुध्यते ।।१८।५।।
अर्थात् जब कर्म और क्लेश नष्ट होते हैं, तब मुक्ति वा बोध का साक्षात्कार होता है। वे कर्म और क्लेश, विकल्प से उत्पन्न होते हैं और विकल्प की उत्पत्ति प्रपंच के प्रभाव से होती है और यह प्रपंच शून्यता में समाप्त हो जाता है।
इसीलिए बौद्ध धर्म (विशेष रूप से महायान बौद्ध धर्म) के अनुसार, केवल शून्यता की प्रत्यक्ष अविकल्प अनुभूति मात्र को बोध वा ज्ञान कहा जाता है, न कि केवल अपने आप को मुक्त होने का विश्वास (दावा) करने पर या केवल वर्तमान क्षण में उपस्थित होने या जागरूकता में रहने पर विश्वास करना, अपने आप में बोध नहीं है। ये बोध वा ज्ञान के केवल पक्ष मात्र हैं पर स्वयं में बोधि नहीं हैं।
यह सब अकेले तो किया जा सकता है लेकिन सम्यक् बोधि केवल ऐसी चीजों की अनुभूतिमात्र नहीं हैं जिसे कर्म और क्लेश से भरा हुआ व्यक्ति जो अपने भीतर की जकड़ी हुई अविद्या से अनभिज्ञ है, प्राप्त कर सके। अनादि अविद्या, किसी अन्य विचार द्वारा जैसे स्वयं को पहले से ही मुक्त सोचकर या वर्तमान में उपस्थित होकर अथवा होशपूर्ण होकर नहीं हटती। उसी तरह जैसे कि मल से भरे दुर्गन्धित हाथ की दुर्गन्ध केवल यह कहने / सोचने / विश्वास करने से कि मेरे हाथों से गंध नहीं आती है या अपने हाथ को होश में रखने से गायब नहीं होती। हालाँकि, ये सभी मार्ग के अभिन्न अंग हैं।
वैसे तो हरेक व्यक्ति बोध, बुद्धत्व वा ज्ञान प्राप्ति की अवस्थाको अपने हिसाबसे परिभाषित करने के लिए स्वतन्त्र है ,लेकिन बुद्ध के अनुसार यह बोधि वा बुद्धता नही है और न ही हजारों वर्षों से अखंडित रूप में सदियों से प्रसारित होती चली आ रही हजारों -हजार ज्ञानलाभी बौद्ध गुरुओं की शुद्ध सिद्ध परम्पराने ऐसे अनुभव को बुद्धत्व माना है। शुद्ध सिद्ध परम्परा के सम्यक् (सही) बौद्ध मार्ग, हजारौं वर्षों से हरेक पीढ़ी में प्रचुर मात्रा में ज्ञानलाभी (ज्ञान लाभ प्राप्त किया हुआ व्यक्ति) व्यक्तियों का उत्पादन करता चला आ रहा है और बौद्ध धर्म में धर्मका अर्थ यही है।
यह एक प्रमाणित राजमार्ग है, जो आजकल के कुछ व्यक्तियों की बोध और बुद्धत्व को लेकर उनकी गढ़ी हुई धारणाओं पर आधारित नव युग-पद्धति के जैसे नहीं है । इस प्रकार की पद्धतियां व्यक्तियों को वास्तविक बोध नदिला सकने के कारण एक-दो पुश्तों में ही लोप हो जाती हैं । विशेषकर , भारतीय उपमहाद्वीप में कईं शताब्दीयों से ऐसी बातें होती चली आ रहीं हैं (ऐसी छत्रक/खुम्बी परम्पराएं उत्पन्न और लोप होती चली आ रहीं हैं )
यह समझना बहुत जरुरी है कि आप भी एक बुद्ध पुरूष (बोध लाभ प्राप्त किया हुआ व्यक्ति) जैसे वर्तमान क्षण में या होश पूर्ण रह सकते हैं पर वर्तमान क्षणमें रहने या अपने होश को निरन्तर कायम रखने पर भी आपको बोध लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। इसके साथ ही ये भी जान लेना अच्छा रहेगा कि बुद्ध ने बताया है कि मिथ्या दृष्टि (गलत आध्यात्मिक परम्परा) तथा मिथ्या समाधि (गलत ध्यान पद्धति) भी होती हैं । सम्यक्संबुद्ध शब्दका अर्थ ही पूर्ण रूपमें , सब प्रकारसे और सही रूपसे (सम्यक् रूपमा) बुद्धत्व लाभ की प्राप्ति है , जो गलत (असम्यक्) बुद्धत्वकी सम्भावनाओं को भी दर्शातिहैं।
अर्थात् ऐसी अवस्थाएँ भी हैं जहाँ ज्ञान या बुद्धत्व लाभ की भ्रान्ति हो सकती है। जब तक मनको क्लेश और अविद्या के बन्धनसे मुक्त न किया जाए तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता और ये चीज़ें किसी गुफा के साधारण अन्धकार जैसी भी नहीं हैं जिसे क्षण भर में दिया जलाकर हटाया जा सके (यह पूर्णतया गलत उपमा का उदाहरण है )। क्लेश और अविद्या का बन्धन हातमें लगे मल के जैसा है जिसे साबुन आदि से अच्छी तरह धोना
चाहिये, वहां पर सहज ज्ञान या तात्कालिक बोधि जैसी कोई चीज नहीं है। बोधि के लिए व्यक्ति को बुद्ध और उनके उपदेशों पर आधारित सम्यक् मार्ग के अनुसार अभ्यास करना जरुरी है।
हालाँकि लोग मन की विभिन्न अवस्थाओं को ज्ञान या बोधि के रूप में कल्पना करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन ऐसी धारणा को बुद्ध द्वारा बताया गया बुद्धत्व मानकर अपने आप को भ्रमित भी न करें। कम से कम जो व्यक्ति स्वयं को बोध प्राप्त करने का दावा करता है, उसे इतना तो स्पष्ट होना ही चाहिए कि बोध का अर्थ प्रतीत्यसमुत्पाद या शून्यता और इनके द्वारा सूचित की गईं सभी चीज़ों (धर्मों )का यथार्थ बोध है।